आधुनिक मीडिया में हिंदी भाषा के स्वरूप की विकासात्मक संभावनाएं!
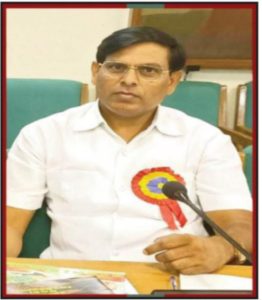
दिनेश कुमार गौड़
लेखक वरिष्ठ पत्रकार एवं “सदस्य” हिन्दी सलाहकार समिति वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार रहे है
समाचार माध्यामों में भाषा का महत्वपूर्ण स्थान होता है। भाषा ही विचारों के आदान-प्रदान का सहज माध्यम है। भाषा एक समाज सापेक्ष क्रिया है, एक सामाजिक व्यवहार है। अतः परिवर्तन शील समाज में भाषा का स्वरूप भी अनुकूलन परक और परिवर्तनीय होता है। इसे हम भाषा का विकासात्मक स्वरूप कहते हैं। कबीर ने हिंदी भाषा को “बहता नीर” की संज्ञा दी थी जो भाषा की एक सटीक और सुस्पष्ट परिभाषा ही है। हिंदी भाषा अपने विकास के लगभग एक हजार वर्षों के इतिहास में निरन्तर बदलती परिस्थितियों, बाध्यताओं और विवशताओं के उतार-चढ़ाव को पार करती हुई सुरसरिता के असन्न प्रवाह की भांति अविरल गति से बढ़ती रही है। हिंदी की प्रकृति सबको साथ लेकर चलने की रही है। विभिन्न भाषाओं के सम्पर्क में आने से इसने अनेक देशी और विदेशी भाषाओं के शब्दों को आत्मसात् किया है इससे इसकी विकास गति प्रबल हुई, सम्प्रेपष्णीयता बढ़ी और यह एक व्यापक व्यापारी भाषा के रूप में विश्व के पटल पर उभरी। इसे सन्तों महात्माओं ने ही अपने विचारों का माध्यम नहीं बनाया, बल्कि देश के स्वतंत्रता आन्दोलन में भी इसकी महती राष्ट्रीय भूमिका रही। गांधी जी और राष्ट्र के अग्रणी नेताओं ने राष्ट्रभाषा के रूप में इसकी पहचान की। इसी दौरान हिंदी के अनेक समाचार पत्रों का जन्म हुआ। स्वतंत्रता संग्राम में हिंदी के समाचार पत्रों का राष्ट्रीय आंदोलन को तेज धार देने में अहम रोल रहा। सच पूछिए तो इसके मानक स्तरूप का विकास भी 19 वीं सदी में राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान ही हुआ। 1826 में उदंत मार्तंड से लेकर हिंदी में जो पत्र-पत्रिकाएं प्रकाशित हुई उन्हीं से हिंदी का एक परिनिष्ठित स्वरूप भी स्थिर हुआ। आज हम वैश्वीकरण की ओर बढ़ रहे है। प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में बड़ी तेजी से परिवर्तन हो रहे हैं। 20 वीं सदी विज्ञान की सदी थी और अब 21 वीं सदी सूचना प्रौद्योगिकी की है। कम्प्यूटर द्वारा संप्रेषण के साधनों में एक नए युग का सूत्र पात हुआ है कहने की आवश्यकता नहीं कि इसकी कार्यक्षमता कितनी विशाल एवं प्रभावपूर्ण है।
आज कम्प्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी दोनों एक दूसरे के पूरक बन चुके हैं। सूचना प्रौद्यौगिकी क्या है ? सूचना को एकत्रित और संसाधित कर उसके संप्रेषण की प्रौद्योगिकी ही सूचना प्रोद्योगिकी है । दूसरे शब्दों में भाषा में सूचना को कोडित, संसाधित, संचारित और इंटरनेट पर, ब्राउजिंग करने के साधन ही सूचना प्रौद्योगिकी की विषय वस्तु हैं। सूचना प्रौद्योगिकी के दो आधार हैं:-
प्रिंट मीडिया, और इलेक्ट्रोनिक मीडिया ।
सूचना प्रोद्योगिकी में माइक्रो इलेक्ट्रोनिक तथा इन्फो इलेक्ट्रोनिक तकनीकों का समावेश होता है। इस में सॉफ़्टवेयर और हार्डवेयर दोनों का प्रयोग शामिल है। सूचना प्रौद्योगिकी अत्यधिक तेज गति से परिवर्तित होने वाली प्रौद्योगिकी है, जो बहुत ही कम समय में उत्पादों को व्यापक रूप में प्रचलित बना देती है। किसी भाषा को व्यापकता प्रदान करने में सूचना प्रौद्योगिकी और कम्प्यूटर का महत्वपूर्ण योगदान है। ओडियो – वीडियो उपकरण अब पत्रकारिता के अभिन्न अंग बन चुके हैं। दूरदर्शन ने जहाँ पत्र को ग्लेमर दिया है, वहीं कम्प्यूटर, इन्टरनेट व अत्याधुनिक साधनों ने समाचार की गति आश्चर्यजनक रूप से बढ़ा दी है। अखबार, पत्र-पत्रिकाएं, रेडियो, कम्प्यूटर, टेलीफोन, फैक्स, ई-मेल, इन्टरनेट आदि सभी का भाषा के साथ गहरा सम्बंध है। पत्र-पत्रिकाओं का प्रकाशन, समाचारों का अखबारों में यथास्थान संकलन और उन्हें चित्रों सहित प्रस्तुत करने में कम्प्यूटरों की सहायता ली जा रही है । कम्प्यूटर द्वारा ही हम किसी समाचार सूचना को एक स्थान से दूसरे स्थान तक इन्टरनेट और ई- मेल द्वारा प्रेषित कर रहे हैं ।
कम्प्यूटर का आविष्कार पश्चिमी देशों में हुआ था । कम्प्यूटर की भाषा पहले अंग्रेजी ही थी। जब यह विकास शील देशों में आया तो लोगों को भ्रम हुआ कि कम्प्यूटर की भाषा अंग्रेजी होने से उनकी भाषाओं का विकास अवरूद्ध हो जाएगा। किंतु कम्प्यूटर तो एक यंत्र है, जो किसी प्रकार की सीमाएं स्वीकार नहीं करता। अंग्रेजी में इसकी लोकप्रियता को शीघ्र ही अन्य भाषाओं ने भांप लिया और अपनी- अपनी भाषाओं में इसका प्रयोग आरंभ किया। आज विश्व की अनेक भाषाओं का कम्प्यूटर पर प्रयोग हो रहा है। हिंदी भी इस दिशा में पीछे नहीं रही। फिर भी, हिंदी भाषा के विश्व में गौरवपूर्ण स्थान को देखते हुए हम कम्प्यूटर के क्षेत्र में अपेक्षित प्रगति नहीं कर पाए हैं। इसके मार्ग में सबसे बड़ी बाधा अंग्रेजी की दासता की मानसिकता वाले वे लोग है जो अंग्रेजी के वर्चस्व को बनाए हुए हैं। वे हिंदी के प्रयोग से कतराते है और वे समय रहते हिंदी के विकास के लिए उपलब्ध आधुनिक और अद्यतन उपकरणों और प्रविधियों के प्रयोग की और अपेक्षित ध्यान नहीं दे रहे हैं। हम कम्प्यूटर का सफल और अधिकतम प्रयोग कर सकें, इसके लिए भाषा के मानकीकरण की सबसे अधिक आवश्यकता है। केन्द्रीय हिंदी निदेशालय ने वर्णमाला और वर्तनी के मानकीकरण की दिशा में कुछ कार्य किया है, जिसे व्यापक रूप से मान्यता मिलनी चाहिए। भाषा विकास के लिए मानकीकरण एक अनिवार्य शर्त है। इसके बिना विश्व की भाषा की दौड़ में हिंदी पीछे रह जाएगी और हम अंग्रेजी के पिछलग्गू ही बने रहेंगे ।
हिंदी अब एक विश्व भाषा के रूप में विकसित हो रही है। भाषाई दृष्टि से देखा जाए तो विश्व में हिंदी जानने वालों की संख्या दूसरे स्थान पर है।
हिंदी भाषा जैसाकि पहले कहा गया है सदैव परिवर्तनशील और विकासशील रही है। कम्प्यूटर और इंटरनेट के आ जाने के बाद इसमें परिवर्तन कल्पनातीत गति से हो रहा है, जो स्वाभाविक ही है। ज्ञान-पोषित समाज में आम जनता की सक्रिय भागीदारी होती है। इसे बढ़ाने और समाज द्वारा प्रौद्योगिकी को तेजी से आत्मसात किए जाने के लिए आवश्यक है कि ज्ञान के आदान-प्रदान में कोई बाधा न आए। हमारी सूचना प्रौद्योगिकी का विकास अंग्रेजी केन्द्रित होने के कारण देश में इसका विकास तेजी से नहीं हो पा रहा है। हिंदी में इन्टरनेट का प्रयोग देरी से अवश्य हुआ, किंतु इस के प्रयोग की सभावनाएं बहुत हैं।
जहाँ तक हिंदी भाषा का प्रश्न है इसके दो स्वरूप है। एक परम्परागत साहित्यिक और दूसरा प्रयोजनमूलक । संविधान में हिंदी को राजभाषा घोषित किए जाने के बाद हिंदी की दुहरी भूमिका हो गई है। पहली साहित्यक, दूसरी प्रशासनिक और बहु प्रयोजनीय, जो आज के युग में अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। आज के उद्योग, प्रौद्योगिकी प्रधान हैं। डॉ० ओमविकास ने आई.एन.एस.डी.ओ.सी. के आंकडों के आधार पर बताया है कि विडंबना यह है कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्रति वर्ष 2.5 • करोड़ पृष्ठों की शोध परक एवं विकास परक जानकारी जुड़ती है, लेकिन हिंदी में नगण्य है। इस विकट और विकराल परिस्थिति से हिंदी जगत को निपटना होगा नहीं तो राष्ट्रीय क्षेत्र में आत्म निर्भरता लोगों की भागीदारी का अभाव रहेगा और देश विकसित नहीं हो सकेगा, कहना न होगा कि हिंदी निदेशालयों और संस्थानों द्वारा प्रतिपादित हिंदी सरल और व्यावहारिक नहीं हो पा रही है। हम अभी भी क्लिष्ठ, दुरूह और भारी भरकम शब्दों के प्रयोग का मोह नहीं छोड़ पा रहे हैं। जन सामान्य की भाषा से कटकर हिंदी का विकास बहुत ही दुष्कर है।
आम आदमी की भाषा ही पत्रकार की भाषा होनी चाहिए। इसे मात्र व्यावसायिक नहीं बनना चाहिए। इसमें सत्य को ढूंढने की सहज प्रवृति का होना आवश्यक है। हमें अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयोग में आ रहे तकनीकी और प्रौद्योगिकी के शब्दों को ग्रहण करने में संकोच नहीं होना चाहिए। संविधान के अनुच्छेद 351 में हिंदी की शब्दावली के सम्बन्ध में पहले ही स्थिति को स्पष्ट कर दिया गया है। किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि हम जान बूझकर अंग्रेजी के ऐसे बेमेल शब्दों का प्रयोग करें, जो जन सामान्य की भाषा से कट कर रह जाएं। जो शब्द हिंदी में पहले से ही प्रयोग में आ रहे हैं, उनके बदले जबरदस्ती अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग फुहड़पन नहीं तो क्या है? मीडिया के लिए इस सम्बन्ध में सतर्कता बरतनी आवश्यक है। समाचार-पत्र, भाषा और ज्ञान के प्रेषक होते है जो समाज के छोटे-बड़े सभी वर्गों तक पहुँचते है। पाठक उनकी भाषा को मानक मान कर उनका अनुकरण करते हैं। किंतु आज के वैश्वीकरण के युग में समाचार पत्रों के सम्पादक विवश नज़र आते हैं। वे भाषा और साहित्य पर ध्यान न देकर अपने स्वामियों के हितों को अधिक प्रश्रय देते है। समाचार पत्र उनके आर्थिक हितों की रक्षा करते हैं। सामाजिक या भाषाई पक्ष अब उनके लिए इतने महत्वपूर्ण नहीं रह गए हैं। यहाँ अनेक उदाहरण हिंदी के दैनिक पत्रों से दिए जा सकते हैं। अन्य भाषाओं के शब्द लेना बुरा नहीं है। हिंदी ने तुर्की, अरबी, फारसी, पुर्तगाली, फ्रेंच और अंग्रेजी के अनेक शब्दों को पहले से ग्रहण किया है। जब अपनी भाषा में उपयुक्त शब्द उपलब्ध हो तो फिर भाषा को दरूह बनाने से क्या लाभ है ? मीडिया कुछ विशेष वर्ग के लिए नहीं है।
लोकतंत्र में लोक भाषा ही जनजन तक पहुँचने का माध्यम है। यह सही है कि आज वैश्वीकरण अथवा भूमंडलीकरण, ‘भूमंडीकरण’ के रूप में आ रहा है। नए-नए बाजार तलाशे जा रहे है। जब अंग्रेजी में विज्ञान से माल नहीं
बिक पाता, तो विवश होकर देश के अधिकांश लोगों की भाषा हिंदी का सहारा लेना पड़ता है। अंग्रेजी के अनेक प्रमुख पत्रों का अपने हिंदी संस्करण निकाला जाना इसका स्वतः प्रमाण है। हिन्दुस्तान ‘नवभारतटाइम्स’ ‘जनसत्ता, ट्रिब्यून, आउट-लुक, इंडिया टुडे आदि पत्र हिंदी में भारी मात्रा में प्रकाशित होते हैं। परिचालन संख्या की दृष्टि से भी हिंदी दैनिकों का स्थान सबसे उपर अर्थात् 40.42 प्रतिशत रहा । हिंदी की पत्र-पत्रिकाएं राष्ट्रीय स्तर पर भारत के अनेक राज्यों से प्रकाशित होती हैं। विदेशों से भी हिंदी पत्र-पत्रिकाएं प्रचुर मात्रा में निकाल रही हैं अमेरिका की पत्रिका ‘स्पैन’अब हिंदी में भी प्रकाशित होती हैं। ब्रिटिश उच्चआयोग द्वारा ‘ब्रिटिश समीक्षा’ हिंदी में निकलती है। क्योंकि हिंदी पाठकों की संख्या अधिक है। समाचार पत्रों के अतिरिक्त अब दवाईयों की शीशियों, श्रृंगार, प्रसाधनों, साबुनों आदि पर हिंदी में भी लिखा जाने लगा है। हिंदी का बाज़ार विस्तृत हैं। ये हिंदी के लिए शुभ लक्षण है। मोबाइल फोन. पर अब हिंदी भी सुनने को मिलने लगी है। मैंने देखा है दिल्ली से अमरीकी विमान सेवाओं में उद्घोषिकाएं सूचनाएं हिंदी में भी देती हैं । इलेक्ट्रोनिक मीडिया में दूरदर्शन के माध्यम से भारत में स्टार प्लस स्टार न्यूज, सोनी, डिस्कवरी, एनिमल वर्ल्ड, आदि तमाम चेनलों ने अपने कार्यक्रम प्रस्तुत करना प्रारंभ किया है। इन सभी चैनलों के कार्यक्रम अंग्रेजी की चास्नी के साथ यहां अवतरित हुए थे, किंतु इन्हें विवश होकर हिंदी की ओर मुड़ना पड़ा। इन्हें तो अपने श्रोताओं की संख्या बढ़ानी थी। अपने विज्ञापन आदि दूर-दराज तक पहुंचाने थे। बी.बी.सी. तो काफी दिनों से हिंदी में समाचार देती आ रही है। आज इलेक्ट्रोनिक मीडिया टी.वी. चेनलों तथा मनोरंजन की दुनिया में हिंदी सबसे अधिक मुनाफे की भाषा बन गई हैं। अनुमान है कि कुल विज्ञापनों का 75 प्रतिशत हिंदी माध्यम में है। कौन बनेगा करोड़ पति ने रिकार्ड तोड़ लोकप्रियता प्राप्त की थी इसमें भागीदारिता निभाने वाले देश के कोने-कोने के लोग थे।
जहां तक सिनेमा और फिल्म जगत का प्रश्न है हिंदी प्रचार-प्रसार में इन का सबसे बड़ा हाथ है। हिंदी न जानने वाले भी हिंदी फिल्मों को देखने में रूचि लेते है। इनसे हिंदी की भारी लोकप्रियता बढ़ी है। इसमें कोई संदेह नहीं है। फिल्मी गीत अनेक देशों में भारत के बाहर भी बड़े चाव से सुने जाते हैं। यहां यह कहना अप्रासंगिक नहीं होगा कि कभी-कभी हिंदी फिल्मों के गीतों में अनावश्यक रूप से अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग हिंदी भाषा की सहज प्रकृति को ही बिगाड़ देता हैं। हिंदी में उपलब्ध सरल शब्दों के बदले अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग अटपटा, तो लगता ही हास्यास्पद’ भी बन जाता है, जैसे यह दिल मांगे ‘मोर’। यहां ‘अधिक’ के लिए’ मोर’का प्रयोग सुनते ही ध्यान पहले ‘मयूर’ पक्षी की ओर जाता है। बाद में अधिक होने की ओर। इस प्रकार के अनेक उदाहरण है। यदि मीडिया और सिनेमा जगत के लोग हिंदी की सहज और स्वाभाविक प्रकृति को ध्यान में रखकर भाषा का प्रयोग करते रहे तो आधुनिक मीडिया में हिंदी भाषा के विकासात्मक स्वरूप की भारी संभावनाएं निहित हैं।
संविधान के अनुसार हिंदी भाषा के विकास और प्रचार-प्रसार की ज़िम्मेदारी भारत सरकार की भी है। किसी ने ठीक ही कहा कि कमज़ोर राष्ट्र कमज़ोर भाषा का निर्माण करते है। (weak nations produce weak languages) इसलिए सरकार को हिंदी के लिए अद्यतन और नवीनतम आवश्यक उपकरण उपलब्ध कराने की और विशेष ध्यान देना होगा। साथ ही शब्दों और फौंट आदि साधनों के मानकीकरण पर भी समय रहते गौर करना होगा। नही तो हम अंग्रेजी की दासता के बोझ से भावी पीढ़ी को मुक्त नहीं करा पाएंगे, क्योंकि भाषाई विकास और आर्थिक समृद्धि एक दूसरे से जुड़े होते हैं।

